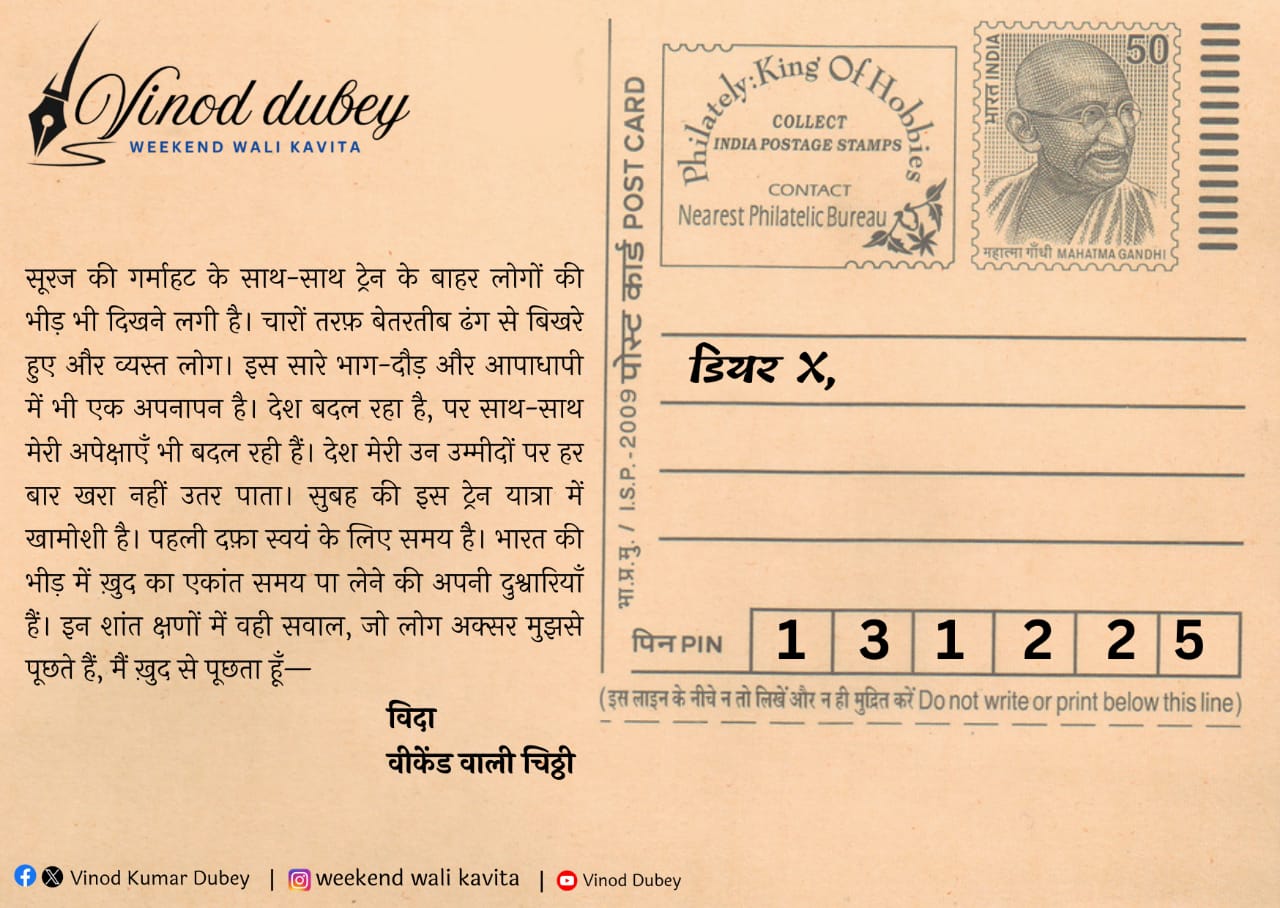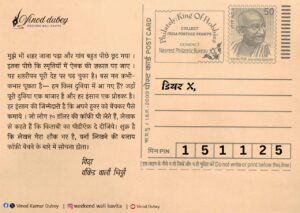डिअर X,
वंदे भारत ट्रेन से बनारस से दिल्ली की यात्रा में हूँ। सुबह का वक्त है। निर्मल वर्मा ने कहा था कि धुंध की भी एक धुन होती है। एकांत के क्षणों में वह सुनाई दे रही है। कुहरे के पीछे किरणें चमक रही हैं। सूरज ट्रेन की खिड़की के शीशे पर कुहासे की कलम से कुछ लिख रहा है। भारतीय रेल यात्रा में जिस भीड़ की उम्मीद थी, लोग उससे कम हैं। सफ़ाई, चाय-नाश्ता और सारा वातावरण विकसित हो रहे भारत की गाथा गा रहे हैं। भारत से उड़े बरसों गुज़र गए, किंतु यह बदलाव सुकूनदेह है। त्रिवेणी संगम के पुल से ट्रेन गुज़र रही है।
सूरज की गर्माहट के साथ-साथ ट्रेन के बाहर लोगों की भीड़ भी दिखने लगी है। चारों तरफ़ बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए और व्यस्त लोग। इस सारे भाग-दौड़ और आपाधापी में भी एक अपनापन है। देश बदल रहा है, पर साथ-साथ मेरी अपेक्षाएँ भी बदल रही हैं। देश मेरी उन उम्मीदों पर हर बार खरा नहीं उतर पाता। सुबह की इस ट्रेन यात्रा में खामोशी है। पहली दफ़ा स्वयं के लिए समय है। भारत की भीड़ में ख़ुद का एकांत समय पा लेने की अपनी दुश्वारियाँ हैं। इन शांत क्षणों में वही सवाल, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं ख़ुद से पूछता हूँ—
“क्या मैं सचमुच भारत लौट आना चाहता हूँ?”
लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट उत्तर दिया जा सकता है, किंतु स्वयं को नहीं। लोगों के प्रश्न को कल पर टाला जा सकता है, किंतु स्वयं के प्रश्न को नहीं। लोगों को बताते समय फ़ैसले को परिवार के हवाले छोड़ा जा सकता है, किंतु मन जानता है कि लोग फ़ैसले को प्रभावित कर सकते हैं, पर अंतिम फ़ैसला आपको ही लेना होता है। सुविधाएँ और आपाधापी, रिश्ते और अकेलेपन की खींचतान में यह निर्णय आख़िर में हमारा ही होता है—कि रस्सी कब पकड़नी है और कब छोड़ देनी है।
जिन्होंने भारत में अपनी परवरिश के दिन बिताए हैं, उनका देश की मिट्टी से जुड़ाव स्वाभाविक है। मानवीय संवेदनाओं से परे यदि आप सिर्फ़ नफ़ा-नुक़सान के बारे में सोच लेते हैं, तो मुबारक हो—आपका फ़ैसला कत्तई आसान होगा। किंतु संवेदनशील इंसान सुविधाएँ तलाशते हुए भी अपनों का हाथ थामे रखना चाहता है। शायद इसीलिए वह हमेशा ऊहापोह की स्थिति में रहता है।
मैं भी उत्तरों के कई करवट बदलने के बाद फ़ैसला कल पर टाल देता हूँ। मैं, मेरा परिवार, आसपास की परिस्थितियाँ और इन सबसे बनी मेरी सोच इस क़दर बदल रहे हैं कि अगले पाँच सालों बाद मैं क्या सोच रहा होऊँगा, मुझे आज बिल्कुल नहीं पता। इसलिए टालना ही उचित है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊँगा, किंतु इतना पता है कि मानचित्र पलटते हुए भारत दिखने पर उँगलियाँ छूने को आतुर न हों—यह अब इस जीवन में संभव नहीं।
धूप खिल गई है। धूप सर्दियों का सुकून है। नीलगायों के झुंड खेतों से गुज़र रहे हैं। छतों पर ऊँघते हुए लोग दिख रहे हैं। इतनी आपाधापी में भी लोग इस क़दर कैसे सुस्ता लेते हैं, सोचकर मुस्करा पड़ता हूँ। शायद इसीलिए इस सारे भाग-दौड़ और आपाधापी में भी एक अपनापन नज़र आता है।
इन चिट्ठियों को कब प्रेषित कर पाऊँगा, नहीं पता; किंतु लिखने का वक्त हर हफ्ते खोज निकालूँगा—यह भरोसा है।
विदा
वीकेंड वाली चिट्ठी