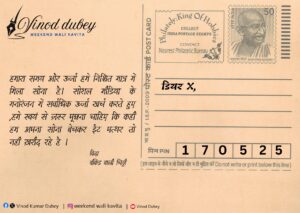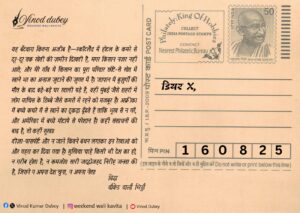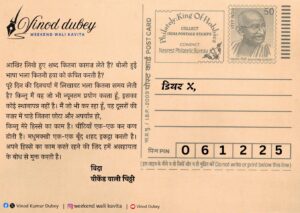Dear X,
कहते हैं कोई काम आप २१ दिन तक करेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि २१ की संख्या को किस सूत्र से निकला गया , किन्तु यह ज़रूर पता है कि हर शाम चिठ्ठियों का हिस्सा लिखते हुए मुझे २१ से ज्यादा दिन हो गए। अब लगता हिअ जैसे चिट्ठियां लिखना मुझे पसंद भी आने लगा है। इन चिट्ठियों में मैं अपनी सोच जस का तस लिख पाटा हूँ । मेरी सोच जो, मैंने अपने अनुभव, आस पास के लोगों, माहौल और अपनी पढ़ाई लिखाई से तैयार की है। मेरी सोच निजी है और इसलिए मैं जो कुछ भी लिखता हूँ उसमे गलत होने की पूरी संभावना होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चिट्ठियों को तुम निष्पक्ष भाव से ही पढ़ो । इनमे गलतियों की पूरी संभावना होगी।
वैसे एक और मज़ेदार बात हुई। मैं नदी के किनारे किसी पेड़ की छाँव में बैठा यह चिट्ठी लिख रहा था। हवाएं थी, फूलों की खुशबू थी और उसी एक खुशगंवार क्षण में मुझे सहसा लगने लगा कि मैं लेखक बन गया । जैसे हवा छूकर गुजर जाती है, अगले ही क्षण मुझे अपनी सोच पर हंसी आयी। न जाने क्यूँ, हमारा बावला मन भ्रम पालने को क्यों आतुर होता है? हम कुछ भी करते हैं, उसमे विशिष्ट होने का भ्रम पालने लगते हैं ।
इस बार मैं अपने लिखने पर सोचता रहा। मुझे लिखना भले पसंद है किन्तु कई बार यह सवाल कौंध उठा कि क्या यह जरूरी है कि हमेशा लिखा जाए? मुझसे पहले कितनों ने कितना कुछ तो लिखा है, मेरे बाद भी कितने लोग कितना कुछ लिखेंगे। अगर मैंने कुछ नहीं भी लिखा तो इस दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। फिर मेरा लिख लेना मुझे कहाँ विशिष्ट बनाता है?
शायद यह मेरे मन की लालसा हो कि ” लेखक ” होकर मैं किसी के मन में अपने प्रति थोड़ा आकर्षण पैदा करने में सक्षम होऊं। पर क्या सचमुच मैं स्वयं के लेखक होने से आकर्षित हूँ? कत्तई नहीं। मेरे पहले, बड़े लेखकों ने जो कुछ लिखा, उसे पढ़ते हुए निसंदेह कह सकता हूँ कि उनके सामने कुछ भी तो नहीं। निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञेय को पढ़ते हुए लगता है जैसा एक बौना ऊँट पहाड़ के सामने खड़ा होकर अपना कद नापने की कोशिश कर रहा हो।
मैं चाहूँ तो एक दलील दे सकता हूँ, कि जीवन के लिए एकाध भ्रम चाहिए होता है। किन्तु मैं जानता हूँ, यह दलील बेहद कमजोर होगी। भ्रम में जीना भी क्या जीना? ऐसा जैसे, पूजा-पाठ में लगा हुआ व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के पास होने का भ्रम पाल बैठे। वैसे इस दुनिया में भ्रम बड़े सटीक तरीके से पाले जाते हैं। अब देखो ना, माता पिता को लगता है कि वे अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। अध्यापक को लगता है कि वह शिष्यों में ज्ञान बाँट रहा है। जबकि यह उनके जीवन के स्वाभाविक कर्म होते हैं।
मेरा लिखना भी तो ठीक वैसा ही एक कर्म है। परन्तु क्या सचमुच मेरा लिखना उतना ही स्वाभाविक है जितना माँ-बाप का बच्चों को पालना या फिर अध्यापक का शिक्षा देना। मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर ” नहीं” है। इस ख़याल से मन पहले थोड़ा आहत हुआ फिर सुकून मिला कि चलो “लेखक” होने का अतिरिक्त बोझ हट गया।
अब शायद लिखते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा लिखना भी एक स्वाभाविक कर्म की तरह हो जाए। प्रेमचंद कहते थे ” मैं दिहाड़ी मज़दूर हूँ, जिस दिन कुछ न लिखूं, मुझे रोटी खाने का हक़ नहीं ” । मैं सोचता रहा कि क्या मैं स्वाभाविकता की इस ऊँचाई तक पहुँच पाउँगा कि लिखते समय मुझे इस बात का रत्ती भर ख्याल नहीं रहे कि मेरा लेखन मुझे विशिष्ट बना देगा। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कोई विशिष्टता ओढ़ी, तो भ्रम आने में देर नहीं करेगा। काश! हम कर्म से आसक्त हुए बिना कर्म कर सकते।
अपनी कुछ पंक्तियाँ तुम्हे सौंपते हुए विदा लेता हूँ:
स्वयं का सम्मान भले करो लेकिन,
श्रेष्ठ होने का वहम मत पालो तुम,
उपलब्धियाँ, त्याग, तपस्या, जैसी,
बेफ़ज़ूल बातों पर मिट्टी डालो तुम,
जो भी जैसा भी जीवन मिला तुम्हें,
उसे आनन्द में जीकर जाना तुम,
तुम्हारे बाद कोई याद रखेगा तुम्हें,
इस ग़लतफ़हमी में मत आना तुम, वीकेंड वाली चिट्ठी