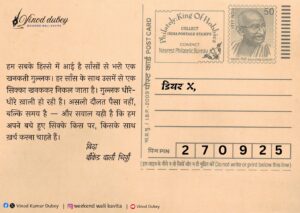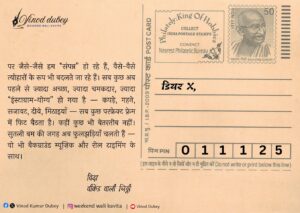Dear X,
फ़िज़ाओं में बसंत की आहट आ चली है। मैं अकेले घूमते हुए प्रकृति में बिखरे सौंदर्य को निरखता हूँ। पेड़ों पर खिले रंग बिरंगे गुच्छेदार फूल देखकर लगता है कि आह! क्यों न कहें बसंत को, ऋतुओं का राजा?
मैं फिर सोचता हूँ कि सौंदर्य का यह खाँचा आख़िर किसने निर्धारित किया होगा? ठूठे पेड़, हवाओं में उड़ते सूखे पत्ते कुरूप और फूलों से लदे हरे भरे पेड़ सुंदर। क्या हेमंत, शिशिर, शरद जैसे ऋतुओं को बसंत से डाह नहीं होगा। पर उन्हें बसंत से क्यूँ, उन कवियों से डाह होना चाहिए जिन्होंने बसंत को सर आँखों पर बिठा लिया। कवि भी क्या करे, वह भी इसी समाज का हिस्सा ही तो है। इसी समाज से निर्मित उसका मन, जहाँ गोरा होना, लंबा होना, सुडौल शरीर होना, बड़ा माथा, नुकीली नाक और ना जाने क्या – क्या सुंदरता की परिभाषा की किताब में लिख दिया गया है ।
कितनी मजेदार बात है कि पैदा होते समय हमारे डीएनए से लेकर बड़े होते वक्त हमारा ख़ान पान, हमारा रहन सहन, हमारी सोच, सबकुछ हम नहीं दूसरे निर्धारित करते हैं। किंतु इन्ही चीज़ों से बनी हमारी शारीरिक रूपरेखा की ज़िम्मेदारी हमारी हो जाती है। अफ्रीकन, एशियन, यूरेपियन, क्या अपनी मौलिक बनावट बदल पायेंगे? हम भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग लगभग एक जैसे ही तो होते हैं किंतु उसी में से हमने कितने विभेद कर लिए हैं।
और इसका नतीजा क्या? हममे से कुछ जीवन लगा देते हैं अपना रंग रूप बदलने में, कुछ अपनी उपलब्धियों के ज़रिए बदला लेना चाहते हैं, और जो कुछ नहीं पर पाते, जीवन भर कमतर होने के अवसाद में जीते हैं। यह कैसी स्पर्धा है जो हमने ईश्वर की बनावट के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है। उसने बड़ी मेहनत से हम सबको यूनिक बनाया और हम सब लग गए एक खाँचे में फिट होने की कोशिश में।
हम अपनी नैसर्गिक बनावट से आख़िर क्यों सहज नहीं रह पाते? हम क्यों नहीं आइने के सामने खड़े होकर कह पाते कि ये मैं हूँ और जैसा भी हूँ यही मैं हूँ और मुझे इसी का ख्याल रखना है। मैं जानता हूँ कि हम समाज की सोच नहीं बदल सकते। समाज को लगता है कि जो सुंदर दिखता है वह अच्छा है। पर हमने देखा है कि ईश्वर का दिया रंग रूप, समय के साथ क्षीण हो जाता है और जिस चरित्र का निर्माण हम स्वयं करते हैं वह जीवन भर वैसे का वैसे रहता है।
हमारा काम था ईश्वर के दिए शरीर का ख्याल रखना ताकि इस शरीर का मनमाफ़िक उपयोग करके हम अपनी इच्छानुसार एक सुंदर जीवन जी सकें। हमने इसमें भी स्पर्धा तैयार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बसर सोचो कि अगर हम दूसरों और स्वयं को रंग रूप, क़द काठी के आधार पर जज करते हैं तो क्या हम सचमुच ईश्वर की बनायी यूनिक कृतियों का आदर कर रहे हैं। अगर यह बात ठीक से समझ आई तो पतझड़ के हवा में उड़ते सूखे पत्ते भी उतने ही ख़ूबसूरत नज़र आयेंगे जितने फूलों के गुच्छों से लदे हरे भरे पेड़। जीवन के हर रंग को उसी सहजता से बिना भेद भाव स्वीकार करना ही ईश्वर का कारीगरी का सम्मान है।
अपनी लिखी कुछ पंक्तियां तुम्हें सौंपते विदा लेता हूँ:
शरीर की बाहरी परतें खरोंच,
क्या आत्मा तक जा पाये तुम,
क्या सचमुच प्रेम किया तुमने,
क्या उसे महसूस करा पाये तुम, वीकेंड वाली चिट्ठी